Master संत कबीर दास की जीवनी
Join thousands of students accessing our vast collection of expertly curated tests, daily quizzes, and topic-wise practice materials for comprehensive exam preparation.
.4b5d1eae.png)
Join thousands of students accessing our vast collection of expertly curated tests, daily quizzes, and topic-wise practice materials for comprehensive exam preparation.
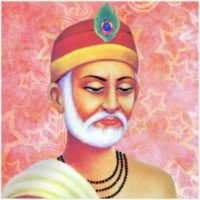
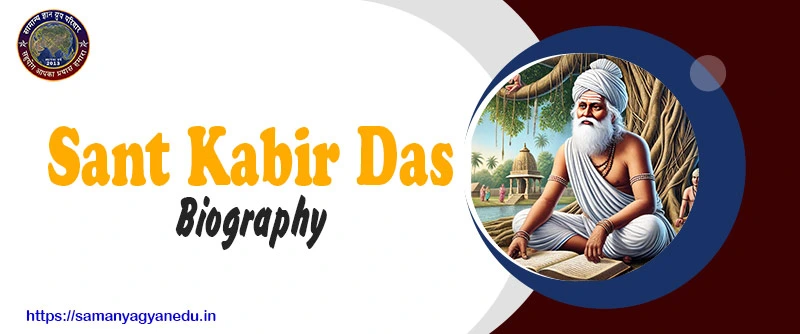
पूरा नाम - संत कबीरदास
अन्य नाम - कबीरा, कबीर साहब
जन्म - सन 1398 ( लगभग )
जन्म - भूमि लहरतारा ताल, काशी
मृत्यु - सन 1518 ( लगभग )
मृत्यु स्थान - मगहर, उत्तर प्रदेश
पालक माता-पिता - नीरु और नीमा
पति/पत्नी लोई, संतान कमाल (पुत्र), कमाली (पुत्री)
कर्म भूमि - काशी, बनारस
कर्म-क्षेत्र - समाज सुधारक कवि
मुख्य रचनाएँ - साखी, सबद और रमैनी
भाषा - अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी
शिक्षा - निरक्षर
नागरिकता - भारतीय
संबंधित लेख कबीर - ग्रंथावली, कबीरपंथ, बीजक, कबीर के दोहे आदि
अन्य जानकारी- कबीर का कोई प्रामाणिक जीवनवृत्त आज तक नहीं मिल सका, जिस कारण इस विषय में निर्णय करते समय, अधिकतर जनश्रुतियों, सांप्रदायिक ग्रंथों और विविध उल्लेखों तथा इनकी अभी तक उपलब्ध कतिपय फुटकल रचनाओं के अंत:साध्य का ही सहारा लिया जाता रहा है।
कबीर साहब एवं संत कबीर जैसे रूपों में भी प्रसिद्ध है। ये मध्यकालीन भारत के स्वाधीनचेता महापुरुष थे और इनका परिचय, प्राय: इनके जीवनकाल से ही, इन्हें सफल साधक, भक्त कवि, मतप्रवर्तक अथवा समाज सुधारक मानकर दिया जाता रहा है तथा इनके नाम पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय भी प्रचलित है। कबीरपंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं और इनके संबंध में बहुत सी चमत्कारपूर्ण कथाएँ भी सुनी जाती हैं।
इनका कोई प्रामाणिक जीवनवृत्त आज तक नहीं मिल सका, जिस कारण इस विषय में निर्णय करते समय, अधिकतर जनश्रुतियों, सांप्रदायिक ग्रंथों और विविध उल्लेखों तथा इनकी अभी तक उपलब्ध कतिपय फुटकल रचनाओं के अंत:साध्य का ही सहारा लिया जाता रहा है। फलत: इस संबंध में तथा इनके मत के भी विषय में बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है।
महात्मा कबीरदास के जन्म के समय में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा शोचनीय थी। एक तरफ मुसलमान शासकों की धर्मांन्धता से जनता परेशान थी और दूसरी तरफ हिन्दू धर्म के कर्मकांड, विधान और पाखंड से धर्म का ह्रास हो रहा था। जनता में भक्ति- भावनाओं का सर्वथा अभाव था। पंडितों के पाखंडपूर्ण वचन समाज में फैले थे। ऐसे संघर्ष के समय में, कबीरदास का प्रार्दुभाव हुआ। जिस युग में कबीर आविर्भूत हुए थे, उसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी।
यह घटना इस्लाम जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदाय का आगमन था। इस घटना ने भारतीय धर्म–मत और समाज व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी अपरिवर्तनीय समझी जाने वाली जाति–व्यवस्था को पहली बार ज़बर्दस्त ठोकर लगी थी। सारा भारतीय वातावरण संक्षुब्ध था। बहुत–से पंडितजन इस संक्षोभ का कारण खोजने में व्यस्त थे और अपने–अपने ढंग पर भारतीय समाज और धर्म–मत को सम्भालने का प्रयत्न कर रहे थे।
कबीर सन्त कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक-एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थपूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया और असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियाँ उड़ाता चला गया। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी पलीता था। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है।
संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं, जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ़ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व - प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है।
जन्म - कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं। कबीर पन्थियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिन्दू धर्म की बातें मालूम हुईं। एक दिन, एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े।
रामानन्द जी गंगा स्नान करने के लिये सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल `राम-राम' शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा-मन्त्र मान लिया और रामानन्द जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में-
हम कासी में प्रकट भये हैं, रामानन्द चेताये।
कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में यह पद्य प्रसिद्ध है-
चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए। जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भए॥
घन गरजें दामिनि दमके बूँदे बरषें झर लाग गए। लहर तलाब में कमल खिले तहँ कबीर भानु प्रगट भए॥
कबीर के जन्मस्थान के संबंध में तीन मत हैं : मगहर, काशी और आजमगढ़ में बेलहरा गाँव।
1. मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख किया है : "पहिले दरसन मगहर पायो पुनि कासी बसे आई अर्थात् काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीर का मक़बरा भी है।
2. कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे काशी के जुलाहे के रूप में ही जाने जाते हैं। कई बार कबीरपंथियों का भी यही विश्वास है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ। किंतु किसी प्रमाण के अभाव में निश्चयात्मकता अवश्य भंग होती है।
3. बहुत से लोग आजमगढ़ ज़िले के बेलहरा गाँव को कबीर साहब का जन्मस्थान मानते हैं।
वे कहते हैं कि ‘बेलहरा’ ही बदलते-बदलते लहरतारा हो गया। फिर भी पता लगाने पर न तो बेलहरा गाँव का ठीक पता चला पाता है और न यही मालूम हो पाता है कि बेलहरा का लहरतारा कैसे बन गया और वह आजमगढ़ ज़िले से काशी के पास कैसे आ गया ? वैसे आजमगढ़ ज़िले में कबीर, उनके पंथ या अनुयायियों का कोई स्मारक नहीं है।
कबीर के माता- पिता के विषय में भी एक राय निश्चित नहीं है। "नीमा' और "नीरु' की कोख से यह अनुपम ज्योति पैदा हुई थी, या लहर तालाब के समीप विधवा ब्राह्मणी की पाप- संतान के रुप में आकर यह पतितपावन हुए थे, ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता है। कई मत यह है कि नीमा और नीरु ने केवल इनका पालन- पोषण ही किया था। एक किवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। एक जगह कबीर ने कहा है :- "जाति जुलाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरो उदासी।'
कबीर के एक पद से प्रतीत होता है कि वे अपनी माता की मृत्यु से बहुत दु:खी हुए थे। उनके पिता ने उनको बहुत सुख दिया था। वह एक जगह कहते हैं कि उसके पिता बहुत "गुसाई' थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विदित होता है कि कबीर अपने वयनकार्य की उपेक्षा करके हरिनाम के रस में ही लीन रहते थे। उनकी माता को नित्य कोश घड़ा लेकर लीपना पड़ता था। जबसे कबीर ने माला ली थी, उसकी माता को कभी सुख नहीं मिला। इस कारण वह बहुत खीज गई थी। इससे यह बात सामने आती है कि उनकी भक्ति एवं संत- संस्कार के कारण उनकी माता को कष्ट था
कबीरदास का लालन-पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उनके मत का महत्त्वपूर्ण अंश यदि इस जाति के परंपरागत विश्वासों से प्रभावित रहा हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यद्यपि 'जुलाहा' शब्द फ़ारसी भाषा का है, तथापि इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ-न-कुछ चर्चा मिलती ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के दसवें अध्याय में बताया गया है कि म्लेच्छ से कुविंदकन्या में 'जोला' या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई है। अर्थात म्लेच्छ पिता और कुविंद माता से जो संतति हुई वही जुलाहा कहलाई।
जुलाहे मुसलमान है, पर इनसे अन्य मुसलमानों का मौलिक भेद है। सन् 1901 की मनुष्य-गणना के आधार पर रिजली साहब ने 'पीपुल्स ऑफ़ इंडिया' नामक एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने तीन मुसलमान जातियों की तुलना की थी। वे तीन हैं: सैयद, पठान और जुलाहे। इनमें पठान तो भारतवर्ष में सर्वत्र फैले हुए हैं पर उनकी संख्या कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। जान पड़ता है कि बाहर से आकर वे नाना स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार बस गए।
पर जुलाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में ही पाए जाते हैं। जिन दिनों कबीरदास इस इस जुलाहा-जाति को अलंकृत कर रहे थे उन दिनों, ऐसा जान पड़ता है कि इस जाति ने अभी एकाध पुश्त से ही मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उन दिनों इस जाति के बचे-कुचे पुराने संस्कार क्या थे।
उत्तर भारत के वयनजीवियों में कोरी मुख्य हैं। बेन्स जुलाहों को कोरियों की समशील जाति ही मानते हैं। कुछेक पंडितों ने यह भी अनुमान किया है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करने वाले कोरी ही जुलाहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कबीरदास जहाँ अपने को बार-बार जुलाहा कहते हैं,
जाति जुलाहा मति कौ धीर। हरषि गुन रमै कबीर।
तू ब्राह्मन मैं काशी का जुलाहा।
वहाँ कभी-कभी अपने को कोरी भी कह गए हैं।
ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि कबीरदास के युग में जुलाहों ने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया था पर साधारण जनता में तब भी कोरी नाम से परिचित थे। सबसे पहले लगने वाली बात यह है कि कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा है, पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपने को 'ना-मुसलमान' कहते रहे। आध्यात्मिक पक्ष में निस्संदेह यह बहुत ऊँचा भाव है, पर कबीरदास ने कुछ इस ढंग से अपने को उभय-विशेष बताया है कि कभी-कभी यह संदेह होता है कि वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं।
उन दिनों वयनजीवी नाथ-मतावलंबी गृहस्थ योगियों की जाति सचमुच ही 'ना-हिंदू ना-मुसलमान' थी। कबीरदास ने कम-से-कम एक पद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं और योगी और हैं, क्योंकि योगी या जोगी 'गोरख-गोरख करता है, हिंदू 'राम-राम' उच्चारता है और मुसलमान 'खुदा-खुदा' कहा करता है।
कबीर बड़े होने लगे। कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे- अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। कबीरदास की खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक़ साधन पिता-माता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त न कर सके।
मसि कागद छूवो नहीं, क़लम गही नहिं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया।
कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या 'लोई' के साथ हुआ था। कबीर को कमाल और कमाली नाम की दो संतान भी थी। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। बूड़ा बंस कबीर का, उपजा पूत कमाल। हरि का सिमरन छोडि के, घर ले आया माल।
कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी बानियों में कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कबीर के घर में रात - दिन मुडियों का जमघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया था। इस कारण से कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। एक जगह कबीर उसको समझाते हैं :- सुनि अंघली लोई बंपीर। इन मुड़ियन भजि सरन कबीर।।
जबकि कबीर को कबीर पंथ में, बाल- ब्रह्मचारी और विराणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रुप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं :- "कहत कबीर सुनहु रे लोई। हरि बिन राखन हार न कोई।।'
यह हो सकता हो कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है :- नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार। जब जानी तब परिहरि, नारी महा विकार।।
कबीर जी ने सोचा कि गुरु किये बिना काम बनेगा नहीं। उस समय काशी में रामानन्द नाम के संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती कीः "मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ।" उस समय जात-पाँत का बड़ा आग्रह रहता था। और फिर काशी ! वहाँ पण्डितों और पाण्डे लोगों का अधिक प्रभाव था। कबीर जी ने देखा कि हर रोज सुबह तीन-चार बजे स्वामी रामानन्द खड़ाऊँ पहनकर 'टप...टप....' आवाज़ करते गंगा में स्नान करने जाते हैं।
कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाड़ कर दी। एक ही मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह के अन्धेरे में कबीर जी सो गये। गुरु महाराज आये तो अन्धेरे के कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया। उनके मुख से उदगार निकल पड़ेः "राम... राम... राम....।" कबीर जी का तो काम बन गया। गुरुजी के दर्शन भी हो गये, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से रामनाम का मंत्र भी मिल गया।
अब दीक्षा में बाकी ही क्या रहा ? कबीर जी नाचते, गाते, गुनगुनाते घर वापस आये। रामनाम की और गुरुदेव के नाम की रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्वक हृदय से गुरुमंत्र का जप करते, गुरुनाम का कीर्तन करते साधना करने लगे। जो महापुरुष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिन्तन करने वाले को भी होने लगती है। काशी के पण्डितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर रामनाम जपता है, रामानन्द के नाम का कीर्तन करता है ! उस यवन को रामनाम की दीक्षा किसने दी ? क्यों दी ? मंत्र को भ्रष्ट कर दिया ! पण्डितों ने कबीर से पूछा:-
"रामनाम की दीक्षा तेरे को किसने दी ?"
"स्वामी रामानन्दजी महाराज के श्रीमुख से मिली।"
"कहाँ दी ?"
"सुबह गंगा के घाट पर।"
पण्डित रामानन्द जी के पास पहुँचे और कहा कि आपने यवन को राममंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, सम्प्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज ! यह आपने क्या किया ?
गुरु महाराज ने कहा- "मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी।"
"वह यवन जुलाहा तो रामानन्द..... रामानन्द.... मेरे गुरुदेव रामानन्द" की रट लगाकर नाचता है, आपका नाम बदनाम करता है।"
"भाई ! मैंने उसको कुछ नहीं कहा। उसको बुलाकर पूछा जाय। पता चल जायेगा।"
काशी के पण्डित इकट्ठे हो गये। कबीर जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं। सामने विद्वान पण्डितों की सभा बैठी है।
रामानन्दजी ने कबीर से पूछाः "मैंने तुझे कब दीक्षा दी ? मैं कब तेरा गुरु बना ?"
कबीर जी बोलेः "महाराज ! उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श कराया और राममंत्र भी दिया, वहाँ गंगा के घाट पर।"
रामानन्द जी कुपित से हो गये। कबीर जी को अपने सामने बुलाया और गरज कर बोलेः "मेरे सामने तू झूठ बोल रहा है ? सच बोल...."
"प्रभु ! आपने ही मुझे प्यारा रामनाम का मंत्र दिया था...."
कबीरदास की मजार और समाधि, मगहर, उत्तर प्रदेश
रामानन्दजी को गुस्सा आ गया। खडाऊँ उठाकर दे मारी कबीर जी के सिर पर।
"राम... राम...राम....! इतना झूठ बोलता है....।"
कबीर जी बोल उठेः "गुरु महाराज ! तबकी दीक्षा झूठी तो अबकी तो सच्ची...! मुख से रामनाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया।"
स्वामी रामानन्द जी उच्च कोटि के संत-महात्मा थे। घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गये। फिर पण्डितों से कहाः "चलो, यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नम्बर का शिष्य यही है।"
ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार कर देती है।
कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिन्दू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिन्दू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई, तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल हिन्दुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने।
मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भाँति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद हैं किन्तु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी (सन 1518 ई.) मानते हैं, लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु 1448 को मानते हैं।
भेष का अंग - कबीर
मधि का अंग - कबीर
उपदेश का अंग - कबीर
करम गति टारै नाहिं टरी - कबीर
भ्रम-बिधोंसवा का अंग - कबीर
पतिव्रता का अंग - कबीर
मोको कहां ढूँढे रे बन्दे - कबीर
चितावणी का अंग - कबीर
बीत गये दिन भजन बिना रे - कबीर
कामी का अंग - कबीर
मन का अंग - कबीर
जर्णा का अंग - कबीर
धन तुम्हरो दरबार - कबीर
माया का अंग - कबीर
कुमिलानी - कबीर
गुरुदेव का अंग - कबीर
नीति के दोहे - कबीर
बेसास का अंग - कबीर
केहि समुझावौ सब जग- कबीर
अन्धा - कबीर
मन ना रँगाए, रँगाए
जोगी कपड़ा - कबीर
भजो रे भैया राम गोविंद- कबीर
हरी - कबीर
सुपने में सांइ मिले - कबीर
तूने रात गँवायी सोय के- कबीर
दिवस गँवाया खाय के - कबीर
मन मस्त हुआ तब क्यों बोलै - कबीर
साध-असाध का अंग - कबीर
दिवाने मन, भजन बिना दुख पैहौ - कबीर
माया महा ठगनी हम जानी - कबीर
कौन ठगवा नगरिया लूटल हो - कबीर
रस का अंग - कबीर
संगति का अंग - कबीर
झीनी झीनी बीनी चदरिया - कबीर
रहना नहिं देस बिराना है - कबीर
साधो ये मुरदों का गांव - कबीर
विरह का अंग - कबीर
रे दिल गाफिल गफलत मत कर - कबीर
सुमिरण का अंग - कबीर
फ़कीरी में मन लाग्यो मेरो यार- कबीर
राम बिनु तन को ताप न जाई - कबीर
तेरा मेरा मनुवां - कबीर
साध का अंग - कबीर
घूँघट के पट - कबीर
हमन है इश्क मस्ताना - कबीर
सांच का अंग - कबीर
सूरातन का अंग - कबीर
मेरी चुनरी में परिगयो दाग पिया - कबीर